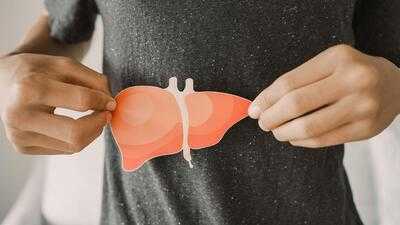लिवर शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है, लेकिन जब ये इस कदर ख़राब हो जाए कि अपना काम ही न कर पाए तो कई मामलों में लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है.
लिवर ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जिसमें ख़राब लिवर को निकालकर उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति, जिसे डोनर कहते हैं, से लिया गया स्वस्थ लिवर या उसका एक हिस्सा लगाया जाता है.
लिवर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत कब पड़ती है? लिवर ट्रांसप्लांट के नियम और शर्तें क्या हैं? लिवर ट्रांसप्लांट के बाद किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए?
ये समझने के लिए हमने लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ़ लिवर ट्रांसप्लांट एंड एचपीबी सर्जरी की कंसल्टेंट और हेड डॉ. विभा वर्मा और दिल्ली के मैक्स सेंटर फ़ॉर लिवर एंड बिलियरी साइंसेज़ के चेयरमैन और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. सुभाष गुप्ता से बात की.
बीबीसी हिंदी के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
कब करवाना पड़ता है लिवर ट्रांसप्लांट? Getty Images लिवर ट्रांसप्लांट के बाद ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि मरीज़ को मिला नया लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं
Getty Images लिवर ट्रांसप्लांट के बाद ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि मरीज़ को मिला नया लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं दोनों ही एक्सपर्ट सिरोसिस, लिवर में शुरू होने वाले कैंसर यानी प्राइमरी लिवर कैंसर, एक्यूट लिवर फ़ेल्योर और बच्चों में कुछ जन्मजात कंडिशन के मामले में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत बताते हैं.
लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. सुभाष गुप्ता कहते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट मुख्य रूप से तीन बीमारियों में किया जाता है.
1. सिरोसिस यानी लिवर पर स्थायी घाव जिससे इसका कामकाज प्रभावित होता है. ये आमतौर पर एल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी से होता है. मोटापा और डायबिटीज़ भी इसके रिस्क फ़ैक्टर हैं.
2. जब लिवर के बाइल डक्ट यानी पित्त की नलियों में समस्या हो, जिसे कोलेस्टेटिक लिवर डिज़ीज़ कहते हैं. इसमें लिवर ठीक होता है, लेकिन इसमें बाइल यानी पित्त का फ़्लो ठीक से नहीं होता.
3. लिवर कैंसर
डॉ. सुभाष गुप्ता बताते हैं कि लिवर कैंसर दो तरह का होता है, प्राइमरी लिवर कैंसर मतलब जब लिवर के अंदर से ही कैंसर शुरू हुआ हो और सेकेंडरी लिवर कैंसर मतलब जब शरीर के किसी दूसरे हिस्से में कैंसर शुरू हो और लिवर तक फैल जाए.
वह कहते हैं कि प्राइमरी लिवर कैंसर में लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है.
डॉक्टर विभा वर्मा बताती हैं, "लिवर ट्रांसप्लांट से सिरोसिस के मरीज़ों में होने वाले कुछ लिवर कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं. कुछ मामलों में, जब कैंसर बड़ी आंत या मलाशय से शुरू हो और केवल लिवर तक फैला हो, ऐसे मामलों में लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है."
इसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांट की चौथी वजह एक्यूट लिवर फ़ेल्योर होता है.
डॉक्टर विभा वर्मा कहती हैं, "एक्यूट लिवर फ़ेल्योर के मामले में इमरजेंसी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है. इसकी वजह कभी-कभी हेपेटाइटिस ए या ई जैसे वायरल संक्रमण हो सकते हैं या कुछ दवाइयां."
- फैटी लिवर: कितना ख़तरनाक और क्या है इसका इलाज?
- महिला के लिवर में तीन महीने का भ्रूण
ट्रांसप्लांट के लिए लिवर मृत डोनर से लिया जा सकता है या जीवित डोनर भी हो सकते हैं.
मृत या ब्रेन डेड डोनर से ट्रांसप्लांट
इसमें डॉक्टर मरीज़ के बीमारी वाले या काम नहीं कर रहे लिवर को निकालकर उसकी जगह डोनेट किया हुआ लिवर लगा देते हैं.
डॉ. विभा वर्मा बताती हैं, "इसमें डोनर का पूरा लिवर मरीज़ में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. या फिर लिवर को दो हिस्सों में कर के एक हिस्सा किसी वयस्क मरीज़ और दूसरा हिस्सा किसी बच्चे को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है."
लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट
एक स्वस्थ व्यक्ति अपने लिवर का एक हिस्सा दान कर सकता है. ऐसे डोनर को लिविंग डोनर कहा जाता है. लिविंग डोनर मरीज़ के परिवार के ही हो सकते हैं.
डॉ. सुभाष कहते हैं, "इसका मतलब ये है कि परिवार का कोई सदस्य लिवर का हिस्सा देगा, उसके अलावा कोई नहीं. जैसे माता या पिता अपने बच्चे को या बच्चे अपने माता या पिता को. पति, पत्नी, भाई, बहन भी लिवर डोनर बन सकते हैं. इसमें भी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन होता है."
डॉ. विभा वर्मा बताती हैं कि भारत में लिवर ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ़ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के अधीन है. इसके अनुसार:
- लिवर डोनर मरीज़ के परिवार का सदस्य होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए और उसे अपनी इच्छा से सहमति देनी चाहिए.
- सरकार से मंज़ूरी वाली एक समिति मरीज़ और डोनर के रिश्ते की पुष्टि करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई दबाव या ज़बरदस्ती न हो.
- कानूनी मंज़ूरी के बाद, डोनर और लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत वाले मरीज़ दोनों की विस्तृत मेडिकल जांच होती है, ताकि इस सर्जरी के लिए उनकी फ़िटनेस की पुष्टि हो सके.
डॉ. विभा वर्मा कहती हैं, "लिविंग डोनर का ब्लड ग्रुप कम्पैटिबल यानी मरीज़ के ब्लड ग्रुप के अनुकूल होना चाहिए. डोनर स्वस्थ होना चाहिए, उसकी उम्र 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए."
लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में डोनर के लिवर का केवल एक हिस्सा लिया जाता है, दाहिना, बायां, या एक तरफ का एक हिस्सा.
समय के साथ डोनर और लिवर पाने वाले दोनों का लिवर अपने पूरे आकार में आ जाता है.
डॉ. सुभाष गुप्ता बताते हैं, "ट्रांसप्लांट के बाद लिवर दो हफ़्ते में लगभग 70 प्रतिशत और एक महीने में लगभग 80-90 प्रतिशत आकार में आ जाता है. डोनर और उसके लिवर का हिस्सा पाने वाले दोनों का लिवर एक साल में अपने 95-100 प्रतिशत आकार में वापस आ जाता है."
डॉ. सुभाष गुप्ता बताते हैं कि भारत में ज़्यादातर लिवर ट्रांसप्लांट लिविंग डोनर से होते हैं.
भारत के नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक़ साल 2024 में देश में 952 मृत डोनर से लिवर ट्रांसप्लांट और 3 हज़ार 946 लिविंग डोनर से लिवर ट्रांसप्लांट किया गया.
डॉ. सुभाष गुप्ता कहते हैं कि भारत में अंगदान को लेकर उतनी जागरुकता नहीं है, जितनी होनी चाहिए.
वह कहते हैं, "अंगदान बहुत ज़रूरी है. इससे बहुत लोगों की जान बच सकती है. आजकल ज़्यादातर लोगों की मृत्यु अस्पताल में होती है, फिर भी अंगदान में बहुत कमी है."
- महिला के लिवर में तीन महीने का भ्रूण
- 'आपके लिवर में बच्चा है', महिला को बताकर डॉक्टर ने क्या सलाह दी
लिवर ट्रांसप्लांट के बाद ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि मरीज़ को मिला नया लिवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं.
इसके लिए डॉक्टर से जांच करवाते रहने की ज़रूरत है. ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर ऑर्गन रिजेक्शन और दूसरी दिक्कतों की जांच करवाते हैं.
ऑर्गन रिजेक्शन क्या होता है?
ऑर्गन रिजेक्शन तब होता है जब शरीर का इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांट किए गए लिवर को "बाहरी" समझकर उसे नष्ट करने की कोशिश करता है. ट्रांसप्लांट के बाद के पहले तीन से छह महीनों में इसकी आशंका सबसे ज़्यादा होती है.
ऑर्गन रिजेक्शन के लक्षण और संकेत क्या हैं?
अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हेल्थ (एनआईएच) के मुताबिक़ असामान्य लिवर ब्लड टेस्ट के ऑर्गन रिजेक्शन का पहला संकेत हो सकते हैं. ऑर्गन रिजेक्शन के संकेत हमेशा ऐसे नहीं होते कि आप उसकी पहचान कर सकें.
एनआईएच के मुताबिक़ ऑर्गन रिजेक्शन के लक्षण जब सामने आते हैं, तो ये हो सकते हैं:
- थकान महसूस होना
- पेट में दर्द बुखार
- त्वचा और आँखों के सफेद भाग का पीला पड़ना
- गहरे रंग का पेशाब
- हल्के रंग का मल
ऑर्गन रिजेक्शन को रोकने के लिए डॉक्टर ऐसी दवाइयां लिखते हैं, जिन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं. ये दवाइयां ट्रांसप्लांट किए गए लिवर के प्रति इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को कम करके ऑर्गन रिजेक्शन को रोकती हैं.
डॉ. विभा वर्मा बताती हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद पहले तीन महीने सबसे नाज़ुक होते हैं क्योंकि इस दौरान इम्यूनोसप्रेसेंट्स के कारण संक्रमण का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है.
उनके मुताबिक़ ऐसे में मरीज़ को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए-
- मरीज़ को मास्क पहनना चाहिए और भीड़-भाड़ वाले या प्रदूषित इलाकों में जाने से बचना चाहिए.
- ऑर्गन रिजेक्शन का रिस्क हो सकता है, जिसका पता ब्लड टेस्ट या लिवर बायोप्सी से लगाया जाता है और इम्यूनोसप्रेसेंट की डोज़ एडजस्ट करके इसका इलाज किया जाता है.
- ट्रांसप्लांट के पहले तीन महीनों के दौरान, भारी शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए.
- इस अवधि के बाद, दवाइयां और फ़ॉलो-अप विज़िट्स धीरे-धीरे कम हो जाती हैं और मरीज़ काम पर लौट सकते हैं.
- समय पर दवाइयां लेना, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ब्लड टेस्ट करवाना और किसी भी असामान्य लक्षण की तुरंत सूचना देना ज़रूरी है.
डॉ. विभा वर्मा कहती हैं कि ज़्यादातर मरीज़ लिवर ट्रांसप्लांट के बाद सामान्य और सक्रिय जीवन जीने लगते हैं.
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, और व्हॉट्सऐप पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)
- हेपेटाइटिस क्या है और कब लिवर फ़ेल हो जाता है?
- दूध पीते ही कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लगता है?
- विटामिन बी12 की कमी आपके शरीर के लिए घातक, खाने में इन चीज़ों को करें शामिल
You may also like

गाजियाबाद में 106 साल पुरानी विंटेज कार ने दर्ज किया इतिहास, आरटीओ में कराया गया विशेष रजिस्ट्रेशन

शनचो-21 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण पूर्णतः सफल रहा

मालदीव ने पूरे देश में ई-सिगरेट को गैरकानूनी घोषित किया

मोनालिसा ने माइक्रो ड्रामा सीरीज में मारी है एंट्री, शेयर किया अपना रोमांटिक वीडियो तो लोग बोले- परफेक्ट जोड़ी

CM Yogi Janata Darshan : गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने सुनी 200 लोगों की फरियादें